भारतेंदु की आलोचना-दृष्टि
भारतेंदु की आलोचना-दृष्टि :— भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का प्रर्वतन युग है, जिसमें साहित्य के विभिन्न रूपों की संरचना में साहित्यस्रष्टाओं ने रुचि ली है। इसलिए कि उन्होंने साहित्य-विषय, साहित्य-रूप, साहित्य-शिल्प और साहित्य-भाषा सभी स्तर पर अपने पूर्ववर्ती साहित्य को प्रकृति और प्रवृति से युग के आग्रह पर परिवर्तन करना चाहा था। इस युग में यही परिवर्तन आलोचना के क्षेत्र में भी दिखता है।
भारतेंदु की आलोचना-दृष्टि
भारतीय आलोचना पद्धति-परंपरा में संस्कृत विद्यागत समालोचक भरतमुनि, राजशेखर, कुंतक, मम्मट आदि से बढ़ती हुई हिंदी में आई। तुलसी की यह उक्ति प्रयोजन ‘कीरति भनिति मूल मलि सोई, सुरसरि सम सब कहूँ हित होई’, काव्य की सैद्धांतिक विवेचना थी तो कबीर की यह उक्ति ‘संस्करित है कूप जल, भाखा बहता नीर’ भाषा की प्रवाहमयता और जीवंतता तथा भाषा के प्रतिमान को स्थापित है करने की कसौटी थी। रीतिकाल में भी ठाकुर और घनानंद आदि ने भी कविता का तत्वगत खंडन किया है।
घनानंद की ‘मोहि तो मोरे कवित्त बनावत’ रचना तथा रचनाकार के मध्य अंतःसंबंध तथा ‘ढेल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीबों कि खेल करि जानो है’ द्वारा ठाकुर ने कारखानों से निकलने वाली बनी-बनाई परिपाटी में कुछ रूढ़िवादी उपमानों के सहारे और अलंकारों से लदी कविताओं की खबर ली है।
भक्तिकालीन और रीतिकालीन आलोचना अपने युगीन साहित्य के मूल्यांकन के लिए निर्मित हुई थी, किंतु हिन्दी साहित्य के आगामी विकास के लिए आलोचना में भी विकास तथा परिवर्तन आवश्यक था। इसीलिए भारतेंदु काल में जहाँ गद्य की अन्य सभी विधाएँ नए सिरे से विकसित की गईं वहाँ हिंदी आलोचना में नए कार्य आरंभ हुए। भारतेंदु के समय तक साहित्यिक विवेचना का स्तर अधिक बौद्धिक हो गया था।
काव्य की आलोचना में तो किसी प्रकार रस और अलंकार पद्धति का प्रयोग हो सकता था। किंतु गद्य साहित्य का मूल्यांकन इसके द्वारा संभव नहीं था। हिंदी में इस समय उपन्यास, कहानी, निबंध आदि गद्य साहित्य का विकास हो रहा था। जिसके मूल्यांकन के लिए नई प्रकार की आलोचना की आवश्यकता थी। तत्कालीन आलोचक अपनी आलोचना में किसी विशेष शास्त्रीय नियम का पालन नहीं कर रहे थे बल्कि वे अपनी रुचि और प्रवृति के अनुसार रचनाओं के गुण-दोष का उद्घाटन कर रहे थे। यह हिंदी आलोचना के विकास का आरंभिक दौर था।
आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में यह लक्षित किया है कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास नाटकों से हुआ जिसे आगे की ओर बढ़ाते हुए यह कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना का सूत्रपात भी 1883ई. में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध ‘नाटक’ से ही हुआ था। इस निबंध में लगभग साठ पृष्ठों में नाटक का शास्त्रीय विवेचन और इतिहास प्रस्तुत किया गया है। यह निबंध दशरूपक, नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, विलसंस हिंदू थियेटर्स, आर्य दर्शन, लायफ ऑव दी एमिनेंट परसंस, हिस्ट्री द इटालिक थियेटर्स, जैसे ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है । इस निबन्ध में भारतेंदु ने नाटक संबंधी अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत किया है।
इस निबंध को उनके शास्त्रीय और सैद्धांतिक समीक्षा-प्रणाली का निबंध कहा जा सकता है। उस युग को देखते हुए यह अपने ढंग का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ निबंध है। इसमें भारतेंदु ने भारतीय नाट्यशास्त्र के नियमों और उनकी प्रक्रियाओं को समझाते हुए बताया है कि नाटक रचना करते समय किन-किन बातों का ध्यान आवश्यक है।
नाटक प्रणयन के सिद्धांत के संबंध में भारतेंदु का कहना है- ‘जिस समय में जैसे सहृदय जन्म ग्रहण करें और देशीय रीति-नीति का प्रभाव जिस रूप में चलता रहे, उस समय में उक्त सहृदयगण के अंत:करण की वृत्ति और सामाजिक रीति-पद्धति इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करना योग्य है।” (भारतेंदु ग्रंथावली, भाग-1 : नाटक, पृष्ठ-714)
भारतेंदु जी ने अपना ‘नाटक’ शीर्षक निबंध में मुख्यतः नाटक-विवेचन करते हुए लिखा है, किंतु उससे उनकी जीवन और साहित्यिक-विषयक धारणाओं का भी पता चलता है। वे साहित्य को शाश्वत सत्ता मानते हुए भी उसमें समाज-सापेक्षता को प्रमुख मानते थे।
उन्होंने इसी निबंध में भारतीय नाटककार कालिदास और अंग्रेजी नाटककार शेक्सपीयर के भाव-विधान की भी तुलना की है और उनकी लोकप्रियता का उल्लेख कर यह प्रतिपादित किया है कि ये लेखक किस प्रकार जन-जीवन के अधिक निकट रहकर अपना साहित्य निर्माण करते हैं। भारतेंदु ने अपने समकालीन आलोचक बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन की भांति अपने समकालीन किसी रचनाकार या रचना की आलोचना नहीं की है।
किंतु उनका ध्यान प्राचीन-साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन की ओर विशेष रूप से गया है। ये साहित्य को विकासशील रूप में देखते हैं। इन्होंने साहित्य का संबंध केवल व्यक्ति से न मानकर साहित्यकार के युग से माना है।
भारतेंदु जी ने साहित्य के उद्देश्य की चर्चा करते हुए दो प्रमुख प्रयोजनों की चर्चा की है। वे हैं आनंद की अनुभूति और लोक हित। भारतेंदु का मानना है कि सहृदय वही हो सकता है जो साहित्यकार के समानांतर उसकी कृति से आनंद प्राप्त कर सके। वामन ने अपने ग्रंथ में सत-साहित्य को सहृदय-प्रीति का कारण बताया था। भारतेंदु ने उसे ही अपनी संपूर्ण परंपरा के साथ विशिष्ट महत्त्व देते हुए तत्काल सहृदय की हृदयानंद निवृत्ति के लिए आनंद को विशिष्ट प्रयोजक ठहराया।
उसका मानना है कि साहित्य की रचना करते समय साहित्य-स्रष्टा को सहृदय के अंत:करण की वृत्ति और सामाजिक रीति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से सहृदय उस रचना से जुड़ जाएगा अन्यथा रचनाकार अपनी बात पहुँचाने में विफल माना जाएगा।
भारतेंदु के रचनात्मक जीवन में 1868ई. से लेकर 1882ई. का समय घोर वैचारिक संक्रमण का समय है। इस दौरान वह धीरे-धीरे दृढ़ होते गए कि भारत के सभी दुख कष्टों का कारण अंग्रेजी राज है। इसीलिए उन्होंने अपनी इस दौर की रचनाओं के द्वारा अंग्रेजी राज की आलोचना करते हुए औपनिवेशिक शोषण को बार-बार ‘एक्सपोज’ किया।
भारतेंदु आधुनिकीकरण का समर्थन करते थे, लेकिन इस समर्थन के बावजूद भी वे अपनी जातीय-सांस्कृतिक विरासत और आत्मपहचान खोने के पक्ष में नहीं थे। वे नहीं मानते थे कि भारत को आधुनिकीकरण की राह पर ले जाने के लिए उपनिवेशवाद जरूरी है, बल्कि बार-बार ‘कर दुःख बढ़े’, ‘पै धन विदेश चलि जात यहै अति ख्वारी’, ‘भीतर-भीतर सब रस चूसै, बाहर से तन मन धन मूसै।
जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखि सज्जन नहि अंगरेज,’ ‘जो भारत जग में रह्यो सबसे उतम देस। ताही भारत में रह्यो अब नहिं सुख को लेस’ जैसी बातें कहकर वे देश की आधुनिक उन्नति और जनता के सुख के मार्ग में अंग्रेजी राज को बाधक मानते थे। इतनी आलोचना के बाद भी वे अंग्रेजों की शिक्षा व रहन-सहन के कायल थे। इसी कारण वे पश्चिम की उपलब्धियों, उसके ज्ञान-विज्ञान से फायदा उठाने की बात कहना नहीं भूलते।
बलिया वाले भाषण में वे खुले मन पर दुख के साथ कहते हैं कि इंग्लैंड में गाड़ी का कोचवान भी अखबार पढ़ता है जबकि यहाँ (भारत) का कोचवान या तो हुक्का पीयेगा या गप्प करेगा। भारतेंदु इस गप्प करने वाली स्थिति के प्रबल विरोधी थे।
शिवप्रसाद सितारे ‘हिंद’ द्वारा लिखित ‘इतिहासतिमिरनाशक’ के तीसरे खंड की आलोचना भारतेंदु ने ‘हरिश्चंद्र मैगजीन’ में 1873ई. में की थी। इसमें उन्होंने इतिहास को सत्ता विमर्श से लोक-विमर्श में रूपांतरित करने की बात की है। इसी में उन्होंने मुस्लिम शासन और अंग्रेजी राज की आलोचना करते हुए लिखा है कि ‘बाबू शिवप्रसाद ने सल्तनत काल में लागू बाईस किस्म के टैक्सो की फेहरिस्त देकर मुसलमानों के दमन-शोषण का वर्णन किया है।
लेखक भूल जाता है कि मध्यकालीन दमन और शोषण की मिसाल लगने वाले वे टैक्स ब्रिटिश शासन में आज भी बदले हुए नामों से जारी हैं। ऊपर से कई ऐसे नए टैक्स भी लग गए, जिनके पहले के अर्धसभ्य शासन कल्पना भी नहीं कर सकते थे।’ इसी आलोचना से उनकी धार्मिक सहिष्णुता का भी पता चलता है। भारतेंदु का आदर-भाव केवल हिंदू धर्म की ओर ही नहीं था बल्कि सभी धर्मों की ओर था। तभी तो इन्होंने इस्लाम के पैंगबर मुहम्मद, उनकी बेटी फातिमा, अली, हसन और हुसैन की जीवनी 1884ई. में ‘पंच पवित्रात्मा’ शीर्षक से लिखी।
भारतेंदु किसी भी धर्म की कट्टरता के खिलाफ थे और उसकी जमकर आलोचना करते थे तभी तो उन्होंने 15 फरवरी 1874 की ‘हरिश्चंद्र मैगजीन’ में ‘अनेक कोटि देवी-देवताओं के माहात्म्य’, ‘छोटी-छोटी बात में ब्रह्महत्या के पाप’, ‘बड़े-बड़े यज्ञ’ और मूल धर्म छोड़कर ‘उपधर्मों’ के आग्रह की आलोचना की थी।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समष्टिगत, नैतिक और सौंदर्य मूल्यों की समष्टि को ही अपना जीवन-दर्शन बनाया। नैतिक एवं समष्टिगत मूल्यों के कारण ही सौंदर्य में उनकी रुचि थी। उनके संपूर्ण साहित्य के अनुसार ही आलोचना में भी युगबोध के अनुरूप समाज-सुधार की भावना बलवती हुई है। वे सत्यप्रतिज्ञा, देश स्नेह आदि समष्टिवादी मूल्यों एवं मर्यादा जैसे नैतिक मूल्यों को उत्तम उद्देश्यफल स्वीकार करते हुए इसे नाटक में आवश्यक मानते हैं।
इसके उदाहरण के लिए वे अपने नाटकों की ही बात करते हैं। ऐसा करने से एक ओर उनकी मूल्य-चेतना स्पष्ट होती है और दूसरी ओर व्यावहारिक समीक्षा भी हो जाती है। इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि ‘आजकल की सभ्यता के अनुसार नाटक रचना में उद्देश्यफल उत्तम निकलना बहुत आवश्यक है। यह न होने से सभ्य शिष्टगण ग्रंथ का तादृश आदर नहीं करते अर्थात् नाटक पढ़ते या देखने से कोई शिक्षा मिले।
जैसे सत्यहरिश्चंद्र देखने से आर्य जाति की सत्यप्रतिज्ञा, नीलदेवी से देश-स्नेह इत्यादि की शिक्षा मिलती है। इस मर्यादा की रक्षा के हेतु वर्तमान समय में स्वकीय नायिका तथा उत्तम गुण विशिष्ट नायक को अवलंबन करके नाटक लिखना योग्य है। यदि इसके विरुद्ध नायिका और नायक के चरित्र हो तो उसका परिणाम बुरा दिखलाना चाहिए। यथा नहुष नाटक में इंद्राणी पर आसक्त होने से नहुष का नाश दिखलाया गया है। अर्थात् चाहे उत्तम नायिका नायक के चरित्र की समाप्ति सुखमय दिखलाई जाय किंवा दुश्चरित्र पात्रों से चरित्र की समाप्ति कंटकमय दिखलाई जाय।
नाटक के परिणाम में दर्शक और पाठक कोई उत्तम शिक्षा अवश्य पावें।’ (भारतेंदु ग्रंथावली: प्रथम भाग, पृष्ठ- 773-774) भाषा के स्वरूप तथा महत्त्व संबंधी इनकी आलोचना विशेष महत्त्व की है। उन्होंने हिंदी साहित्य का अध्ययन भाषा-विज्ञान की दृष्टि से करने पर जोर दिया है तथा शब्दाडंबर को निंदनीय माना है। उनका विचार है कि काव्य की भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वे अपने युग के अन्य आलोचकों की भांति-स्वभावोक्ति को सत्काव्य का लक्ष्य मानते हैं।
इसीलिए उन्होंने रीतिकालीन काव्य का मूल्यांकन स्वभावोक्ति के आधार पर करते हुए कहा है कि ‘इस समय के कवियों का चित्त स्वभावोक्ति पर तनिक नहीं जाता था। केवल बड़े-बड़े कवि शब्दाडंबर करते थे और इन शब्दाडंबरों वालों का पद्माकर राजा है और इसने वर्ण-मैत्री के हेतु अनेक व्यर्थ शब्द अपने काव्य में भर लिए हैं और इनकी देखा-देखी और भी कवि ऐसा करने लगे? (कवि वचन सुधा, अगस्त 1882)। उन्होंने अतिआलंकारिकता को काव्य के लिए निंदनीय माना है तथा भाषा विज्ञान और भाषा के विकास का भी विवेचन किया है जो कि अपनी आरंभिक अवस्था में थी।
भाषा को एक स्थिर गति देने के लिए भारतेंदु ने ‘हिंदी भाषा’ शीर्षक समालोचनात्मक निबंध लिखा जिसमें उन्होंने भाषा के तीन रूप (घरेलू भाषा, कविता की भाषा और गद्य की भाषा) के संदर्भ के बात की। घरेलू भाषा को तो उन्होंने स्थान-स्थान पर बदलने वाली कहा है। कविता की भाषा के रूप में उन्होंने ब्रजभाषा स्वीकार करते हुए ब्रजभाषा के माधुर्य की बात की है।
गद्य की भाषा के रूप में उन्होंने खड़ी बोली की बात की है। साहित्य भाषा के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन करते हुए उन्होंने उसके शब्द प्रयोगों के अनुरूप शुद्ध तत्सम रूप, सामान्य तद्भव रूप तथा अन्य भाषाओं जैसे फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों को लेकर चलने वाली जनसाधारण की भाषा के रूप का भी विश्लेषण किया है। उनकी मान्यता में भाषा का प्रामाणिक रूप इसी में है कि यह सब प्रकार के शब्दों को अपनी पाचन शक्ति के द्वारा आत्मसात करती हुई चले।
भारतेंदु ‘निज भाषा’ के समर्थक थे लेकिन वे इस निज भाषा को केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं देखना चाहते थे। वे इसे राज-काज की भाषा, विज्ञान की भाषा, ज्ञान की भाषा बनाना चाहते थे। इस संदर्भ में वे आजीवन काम करते रहे।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतेंदु के साहित्य में आलोचना अपने परिपक्व रूप में भले ही न हो लेकिन यत्र-तत्र उनकी समालोचनात्मक प्रज्ञा के दर्शन हो ही जाते हैं जो आज की विकसित बौद्धिक चेतना के सम्मुख एक नवीन विधा के रूप में दृष्टिगत होता है। भारतेंदु जिस समय लिख रहे थे उस समय हिंदी साहित्य में आलोचना की नवीन प्रणाली का कोई विधान नहीं था, उस समय उन्होंने अपने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन से उसका नव-निर्माण किया।
समष्टिगत, नैतिक एवं सौंदर्य मूल्यों का जो समन्वय भारतेंदु ने किया, आगे चलकर वहीं हिंदी आलोचना का मूलधार बना। इसी महत्त्व को रेखांकित करते हुए जार्ज ग्रिर्यसन भारतेंदु को उत्तर भारत के सबसे बड़े आलोचक की संज्ञा प्रदान करते हैं। इस तरह आधुनिक हिंदी आलोचना के प्रवर्त्तन में उनकी महत्ता असंदिग्ध है।

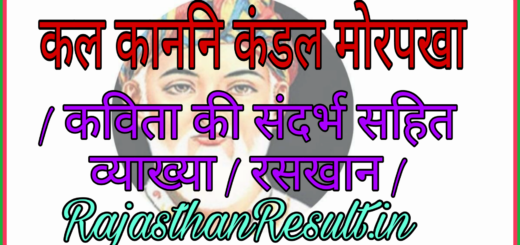


Recent Comments