तुलसीदास की भाषा और काव्य सौंदर्य
तुलसीदास जिस प्रकार अपनी भक्ति में विनयशील हैं उसी प्रकार की विनयशीलता और संकोच उनमें अपनी कवित्व क्षमता के प्रति भी है। ‘रामचरितमानस‘ के बालकांड में अपने इस संकोच को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है :-
तुलसीदास की भाषा और काव्य सौंदर्य
आखर अरथ अलंकृति नाना।
छंद प्रबंध अनेक बिधाना।।
भाव भेद रस भेद अपारा ।
कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा
कबित बिबेक एक नहिं मोरें।
सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें।।
अर्थात भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्द हैं, उनके अर्थ को समझते हुए भावानुकूल शब्द चयन की जिम्मेवारी कवि पर होती है। कविता को अनेक प्रकार से सजाया जाता है; साते हुए भानुकल साथ ही और भय से मन छंद और प्रबंध की तमाम कोटियाँ हैं; उनके अलग-अलग मानदंड हैं। रस और भाव के अने भेद हैं। कविता में विभिन्न प्रकार के गुण और दोष होते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि उनमें काव्य-रचना के इन व्यवहारों का विवेक नहीं है।
वे केवल अनुभूति के सत्य को व्यक्त करने का दावा करते हैं। लेकिन उनकी कविता से गुजरने पर पता चलता है कि काव्य की चारुता और उत्कर्ष के लिए जो भी मानदंड उस समय तक विकसित हुए थे, उन सभी का सुंदर और संयमपूर्ण समायोजन तुलसीदास की कविता में हुआ है। यही कारण है कि रस, अलंकार, शब्द प्रयोग, रूपगत विविधता के बावजूद उनमें कहीं भी शिल्पगत पच्चीकारी दिखाई नहीं देती। अनेक रीतिवादी कवियों की तरह उनकी कविता में भाषागत-शिल्पगत आडंबर नहीं है।
भाषा के स्तर पर तुलसीदास उस समय हिंदी में काव्य भाषा के रूप में प्रचलित अवधी और ब्रजभाषा- दोनों में निष्णात हैं। अवधी तुलसीदास की अपनी भाषा थी, लेकिन ब्रजभाषा में भी उन्होंने अवधी के समान ही भाषागत दक्षता का परिचय दिया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा श्यामसुंदर दास- दोनों का मानना है कि इन दोनों भाषाओं में तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रजभाषा तथा अवधी पर तुलसीदास के अधिकार को रेखांकित करते हुए श्यामसुंदर दास ने लिखा है, “इन दोनों भाषाओं पर उनकी रचनाओं में इतना अधिकार दिखाई देता है कि जितना स्वयं सूरदासजी का ब्रजभाषा पर और जायसी का अवधी पर न था।”
तुलसीदास की कुल बारह रचनाओं में से छह रचनाएँ अवधी में हैं तथा अन्य छह ब्रजभाषा में हैं। अवधी में लिखी गई रचनाएँ हैं- ‘रामलला नहछू’, ‘रामाज्ञाप्रश्न’, ‘जानकी मंगल’, ‘पार्वती मंगल’, ‘बरवैरामायण’ तथा ‘रामचरितमानस’; जबकि ब्रजभाषा में लिखी गई रचनाएँ हैं- “वैराग्य संदीपनी’, “विनय-पत्रिका’, ‘गीतावली’, ‘दोहावली’, ‘कृष्णगीतावली’ तथा ‘कवितावली’ | तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में इन दोनों भाषाओं को निखारा है। जायसी ने ब्रजभाषा के ठेठ रूप का इस्तेमाल किया है, पर तुलसीदास ने तत्सम शब्दों के साथ अवधी का प्रयोग कर भाषा को कलात्मक स्वरूप प्रदान किया। उदाहरणस्वरूप :—
जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँ मति भोरि।
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ।।
तुलसीदास की यही विशिष्टता ब्रजभाषा के संबंध में देखी भी जा सकती है। ‘विनय-पत्रिका’ की इन पंक्तियों को देखिए :—
श्रुति-गुरु-साधु-समृति-संमत यह दृश्य असत दुखकारी।
तेहि बिनु तजे, भजे बिनु रघुपति, बिपति सकै न टारी ।।
काव्य भाषा के रूप में अवधी तथा ब्रजभाषा का प्रयोग करने के साथ ही तुलसीदास ने विभिन्न भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों से अपनी भाषा को समृद्ध किया है। उदाहरणस्वरूप
साहिब उदास भये दास खास खीस होत
मेरी कहा चली? हौं बजाय जाय रह्यौ हौं ।।
यहाँ अरबी के ‘साहिब’ शब्द का तुलसीदास ने ब्रजभाषा के साथ सहजतापूर्ण प्रयोग किया है।
तुलसीदास अपने समय-समाज के लोक जीवन से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। इस कारण जन-व्यवहार में रचे बसे मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग उनकी भाषा की एक प्रमुख विशिष्टता है। उदाहरणस्वरूप :—
तुलसी उराउ होत रामको सुभाउ सुनि,
को न बलि जाइ, न बिकाइ बिनु मोल को।
तुलसीदास की भाषा की सर्वप्रमुख विशेषता है- भाषा का अलंकृत प्रयोग । यद्यपि तुलसीदास गया जा ने कविताओं में अलंकार का सायास प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अलंकार का सौंदर्य उनके काव्य में सहज रूप से सर्वत्र विद्यमान है। वैसे तो तुलसीदास की कविताओं में अनेक प्रकार के अलंकारों की मौजूदगी है, परंतु अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि की योजना प्रमुखता से हुई है।
अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति से भाषा में सौंदर्य पैदा किया जाता है। तुलसीदास के काव्य में अनुप्रास बारंबार दिखाई देता है :
दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।।
काल कराल ब्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि ।।
उपमा अलंकार में दो वस्तुओं के बीच साधर्म्य दिखाया जाता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है। रूपक में उपमेय पर उपमान के आरोप के द्वारा अभेद प्रदर्शित किया जाता है। तुलसीदास के काव्य में इन तीनों अलंकारों का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। यथा:
उपमा :— सुनत सुधासम बचन राम के | गहे सबनि पद कृपाधाम के।।
उत्प्रेक्षा :— सूखहिं अधर जरइ सबु अंगू। मनहूँ दीन मनिहीन भुअंगू। सरूष समीप दीखि कैकेई । मानहुँ मीचु धरी गनि लेई ।।
(राजा दशरथ के सभी अंगों में जलन हो रही थी और ओठ सूख गए थे, मानो साँप मणि को खोकर दुखी हो रहा हो। उनके पास क्रोधित कैकेयी ऐसी दीख रही थी मानो मृत्यु दशरथ के जीवन की अंतिम घड़ी को गिन रही हो।)
रूपक :— कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा।। ह न लग धुन को अस धीरा।।
(शरीर लकड़ी है और मनोकामनाएँ (लालसाएँ) कीड़ा है। ऐसा कौन धैर्यवान है जिसके शरीर में यह घुन (कीड़ा) न लगा हो।
तुलसीदास की काव्य भाषा में विभिन्न संदर्भो में प्रतीकात्मकता का भी संयोजन हुआ है। तुलसीदास ने राम के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता को दिखाने के लिए चातक और पपीहे का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है :—
चढ़त न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के दोष ।
तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख ।।
(मेघ (वर्षा) राम की अनुकंपा है और तुलसीदास की भक्ति चातक की प्रतीक्षा। वे अपने आराध्य के प्रति मन में मलिनता नहीं लाते। राम के प्रति उनके प्रेम की माप-तौल नहीं हो सकती है।)
भाषा की अब तक उल्लिखित विशिष्टताओं के अतिरिक्त तुलसीदास के काव्य सौंदर्य की एक प्रमुख विशिष्टता उनके काव्य-रूप की विविधता में भी निहित है। उन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएँ की हैं। ‘रामचरितमानस’ महाकाव्य है तो ‘रामलला नहछू’, ‘जानकी मंगल’ और ‘पार्वती मंगल’ खंडकाव्य हैं। ‘दोहावली’ ‘कवितावली’, ‘विनय-पत्रिका’ आदि मुक्तक ,काव्य हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ‘कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान’ को तुलसीदास की प्रमुख विशिष्टता के रूप में रेखांकित किया है। तुलसीदास के काव्य में विभिन्न रसों की समुचित योजना की गई है। उदाहरणस्वरूप राम-कौशल्या प्रसंग में वात्सल्य रस, लक्ष्मण शक्ति प्रसंग में करुण रस, नारद-मोह प्रसंग में हास्य रस, शिव-पार्वती विवाह तथा पुष्पवाटिका प्रसंग में शृंगार रस की योजना देखी जा सकती है। तुलसीदास ने शृंगार, खासकर संयोग शृंगार का वर्णन बहुत ही मर्यादित ढंग से किया है।
सारतः हम कह सकते हैं कि तुलसीदास अपनी भक्ति पद्धति एवं सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ भाषा एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी अद्वितीय कवि हैं।
यह भी पढ़े 👇
- ‘रामचन्द्रिका’ की प्रबन्धात्मकता पर विचार व्यक्त कीजिये तथा उसके गुण-दोषों की समीक्षा कीजिये।
- संगम काल में साहित्य के विकास पर प्रकाश डालें।
- दोनों ओर प्रेम पलता है कविता की व्याख्या कीजिए ‘श्री मैथिलीशरण गुप्त’
अपने दोस्तों के साथ शेयर करे 👇


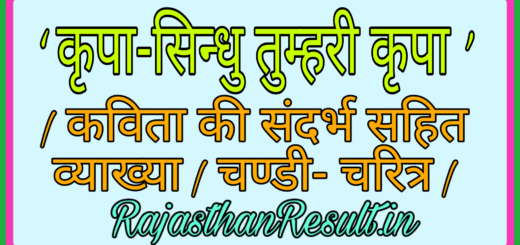

Recent Comments